 स्वामी विवेकानन्द का जन्म 12 जनवरी 1863 विद्वानों के अनुसार विक्रम सवंत1920 की मकर सक्रांति)कोकलकत्तामें हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेन्द्रनाथ दत्त था।पिताविश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्धवकीलथे। विश्वनाथ दत्त पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। वे अपने पुत्र नरेन्द्र को भीअँग्रेजीपढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के ढर्रे पर चलाना चाहते थे। परन्तु नरेंद्र कीमाताभुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थीं। दुर्भाग्य से1884 में विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई। घर का भार नरेन्द्र पर आ पड़ा। घर की आर्थिक अवस्था बहुत दयनीय हो गई थी। अत्यन्त दरिद्रता में भी नरेन्द्र बड़े अतिथि-सेवी थे। वे स्वयं भूखे रहकरअतिथिको भोजन कराते स्वयं बाहर वर्षा में रात भर भीगते-ठिठुरते पड़े रहते और अतिथि को अपने बिस्तर पर सुला देते। स्वामी विवेकानन्द अपना जीवन अपने गुरुरामकृष्ण परमहंसको समर्पित कर दिया | जब रामक्रष्ण परमहंस बहुत बीमार हो गये तब नरेंद्र ने अपने घर और परिवार की नाजुक हालत व स्वयं के भोजन की चिन्ता किये बिना वेगुरुकी सेवा में दिन-रात संलग्न रहे। विवेकानन्द बड़े स्वप्नदृष्टा थे। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें जाति या धर्मके आधार पर किसी से भेदभाव नहीं हो।
स्वामी विवेकानन्द का जन्म 12 जनवरी 1863 विद्वानों के अनुसार विक्रम सवंत1920 की मकर सक्रांति)कोकलकत्तामें हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेन्द्रनाथ दत्त था।पिताविश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्धवकीलथे। विश्वनाथ दत्त पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। वे अपने पुत्र नरेन्द्र को भीअँग्रेजीपढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के ढर्रे पर चलाना चाहते थे। परन्तु नरेंद्र कीमाताभुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थीं। दुर्भाग्य से1884 में विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई। घर का भार नरेन्द्र पर आ पड़ा। घर की आर्थिक अवस्था बहुत दयनीय हो गई थी। अत्यन्त दरिद्रता में भी नरेन्द्र बड़े अतिथि-सेवी थे। वे स्वयं भूखे रहकरअतिथिको भोजन कराते स्वयं बाहर वर्षा में रात भर भीगते-ठिठुरते पड़े रहते और अतिथि को अपने बिस्तर पर सुला देते। स्वामी विवेकानन्द अपना जीवन अपने गुरुरामकृष्ण परमहंसको समर्पित कर दिया | जब रामक्रष्ण परमहंस बहुत बीमार हो गये तब नरेंद्र ने अपने घर और परिवार की नाजुक हालत व स्वयं के भोजन की चिन्ता किये बिना वेगुरुकी सेवा में दिन-रात संलग्न रहे। विवेकानन्द बड़े स्वप्नदृष्टा थे। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें जाति या धर्मके आधार पर किसी से भेदभाव नहीं हो।
स्वामी विवेकानन्दजी का राष्ट्र उत्थान में योगदान
विवेकानन्द की अंतरात्मा इस बात से आश्वस्त थी कि धरती की गोद में यदि ऐसा कोई देश है जिसने मनुष्य के सर्वाधिक विकास की हर सम्भव कोशिश की हैं, तो वह देश मात्र भारत ही है।
विवेकानन्द मात्र सन्त ही नहीं थे किन्तु वे एक महान देशभक्त, श्रेष्ट वक्ता, मूलविचारक, प्रख्यात् लेखक एवं मानवतावादी भी थे। अमेरिका से लौटकर उन्होंने भारतवासियों को आह्वान करते हुए कहा था “नया भारत निकल पड़े मोची की दुकान से, भड़भूँजे के भाड़ से, कारखाने से, हाट से, बाजार से; निकल पडे झाड़ियों, जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों से।” और भारत की जनता भी स्वामीजी के आह्वान पर अपने उत्थान हेतु गर्व के साथ निकल पड़ी। स्वामी के वाक्य”‘उठो, जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ, अपने मानव जीवन को सफल करो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाये” भारतवासी स्वामीजी के आह्वान को अपने मानस पटल पर अकिंत कर अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रगति के पथ पर चल पड़े |
स्वामी विवेकानन्द पुरोहितवाद, धार्मिक आडम्बरवाद, कठमुल्लापन और रूढ़ियों के सख्त विरोधी थे। उन्होंने धर्म को मानव मात्र की सेवा के केन्द्र में रखकर ही आध्यात्मिक चिंतन-मनन किया था। उनका हिन्दू धर्म अटपटा, रुढीवादी एवं अतार्किक मान्यताओं मानने वाला नहीं था। स्वामीजी ने उस समय क्रांतिकारी विद्रोही बयान देते हुए कहा कि “ इस देश के तैंतीस करोड़ भूखे, दरिद्र और कुपोषण के शिकार लोगों को देवी देवताओं की तरह मन्दिरों में स्थापित कर दिया जाये और मन्दिरों से देवी देवताओं की मूर्तियों को हटा दिया जाये “। उनका यह आह्वान आज भी एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। उनके इस आह्वान को सुनकर उस समय सम्पूर्ण पुरोहित वर्ग की घिग्घी बँध गई थी। आज कोई नामी गिरामी साधु तो क्या सरकारी मशीनरी भी किसी अवैध मन्दिर की मूर्ति को हटाने का जोखिम नहीं उठा सकती। विवेकानन्द ने पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद, धार्मिक कर्मकाण्ड और रूढ़ियों की खिल्ली भी उड़ायी और लगभग आक्रमणकारी भाषा में ऐसी विसंगतियों के खिलाफ युद्ध भी किया। स्वामीजी ने संकेत दिया था कि विदेशों में भौतिक समृद्धि तो है और उसकी भारत को जरूरत भी है लेकिन हमें याचक नहीं बनना चाहिये। हमारे देश के पास उससे ज्यादा बहुत कुछ है जो हम पश्चिम को दे सकते हैं और पश्चिम को उसकी अत्याधिक जरूरत है। स्वामी विवेकानन्द का यह कथन अपने देश की धरोहर के लिये दम्भ या बड़बोलापन नहीं था किन्तु एक सच्चे वेदान्ती संत की भारतीय सभ्यता और संस्कृति की तटस्थ, वस्तुपरक और मूल्यगत आलोचना थी।
स्वामी विवेकानन्द के अनुसार व्यक्ति का वास्तविक जन्म ध्येय के प्रगटन के साथ ही होता है। वे कहा करते थे, “जिसके जीवन में ध्येय नहीं वह तो खेलती-गाती, हँसती-बोलती लाश ही है।”जब तक व्यक्ति अपने जीवन के विशिष्ट ध्येय को नहीं पहचान लेता तबतक तो उसका जीवन व्यर्थ ही है। युवको अपने जीवन में क्या करना है इसका निर्णय उन्हें ही करना चाहिये।
स्वामी विवेकानन्द परमात्मा में विश्वास से अधिक अपने आप पर विश्वास करने को अधिक महत्व देते थे। स्वामीजी कहा करते थे कि ” रुढीवादी धर्मावलम्बी कहते है कि ईश्वर में विश्वास ना करनेवाला नास्तिक है किन्तु मै कहता हूँ कि जिस मनुष्य का अपने आप पर विश्वास नहीं है वो ही नास्तिक है” | स्वामीजी ने कहा कि जीवन में हमारे चारो ओर घटने वाली छोटी या बड़ी, सकारात्मक या नकारात्मक सभी घटनायें हमें अपनी असीम शक्ति को प्रगट करने का अवसर प्रदान करती है।
स्वामी विवेकानन्द के अनुसार “किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिये समर्पण अनिवार्य है “। स्वामीजी इसे अध्यवसाय की संज्ञा देते थे। “अध्यवसायी आत्मा कहती है कि मै सागर को पी जाउंगी। उस सींप की भांति जो स्वाती नक्षत्र की एक बुन्द को प्राशन करने के लिये ही लहरों के उपर आती है। एक बुन्द पा जाने के बाद सागर की अतल गहराई में जा बैठती है धैर्य के साथ जब तक उसका मोती ना बन जाये। हमारे युवाओं को ऐसे अध्यवसाय की आवश्यकता है।
स्वामी विवेकानन्द अमरिका में संगठित कार्य के चमत्कार से प्रभावित हुए थे। उन्होंने ठान लिया था कि भारत में भी इस संगठन कौशल को पुनर्जिवित करना है।उन्होंने स्वयं रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर सन्यासियों तक को संगठित कर उन्हें समायोचित उत्तम कार्य करने का प्रशिक्षण दिया था।
“स्वामीजी के जीवन से अनेकों महापुरुषों के जीवन को प्रभावित किया है। आज भी स्वामीजी का साहित्य किसी अग्निमन्त्र की भाँति पढ़नेवाले के मन में कुछ कर गुजरने का भाव संचारित करता है। किसी ने ठीक ही कहा है – यदि आप स्वामीजी की पुस्तक को लेटकर पढ़ोगे तो सहज ही उठकर बैठ जाओगे। बैठकर पढ़ोगे तो उठ खड़े हो जाओगे और जो खड़े होकर पढ़ेगा वो व्यक्ति सहज ही सात्विक कर्म में लग कर अपने लक्ष्य पूर्ति हेतु ध्येयमार्ग पर चल पड़ेगा।
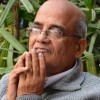
प्रस्तुतिकरण एवं सकलंकर्ता—डा.जे. के. गर्ग
सन्दर्भ—गूगल सर्च, विकीपीडिया,मुक्त ज्ञान कोष, भारत ज्ञान कोष आदि
Please visit our blog—gargjugalvinod.blogspot.in

